प्रमोद भार्गव
इसबार पूरे देश में गेहूं समेत अन्य फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। पूरे देश में 29.19 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है। यह आबादी की जरूरत से 7 करोड़ टन ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भी हर बार की तरह इस साल भी गेहूं की जबरदस्त पैदावार हुई है। समर्थन मूल्य पर 1 करोड़ 25 लाख 88 हजार 986 टन गेहूं खरीदा जा चुका है लेकिन इसके भंडारण का संकट पैदा हो गया है। करीब 11 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है। निसर्ग तूफान के प्रभाव के चलते हुई बारिश से खुले में पड़ा गेहूं बड़ी मात्रा में खराब हो गया। सरकार का दावा है कि महज 0.13 प्रतिशत गेहूं खराब हुआ है। इस भीगे गेहूं का भी सुखाकर भंडारण किया जा रहा है। लेकिन मिली खबरों के मुताबिक सच्चाई इससे जुदा है। दरअसल मध्य-प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बारिश से गेहूं भीगा है। देश के गोदाम पहले से भरे पड़े हैं। मध्य-प्रदेश के गोदामों में ही गेहूं, चना, मूंग, धान सहित दो करोड़ टन अनाज भरा पड़ा है। 80 लाख टन अनाज ऐसा है, जो एक साल से भी ज्यादा समय से रखा हुआ है। इस अतिरिक्त अनाज को भरने के लिए न तो बोरों का प्रबंध है और न ही गोदामों में जगह। इसके भंडारण के लिए जिला कलेक्टर रेलवे स्टेशन, हवाई पट्टी और मंडी के टीनशेडों में जगह तलाश रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर ने हवाई पट्टी पर गेहूं के भंडारण की अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांगी है। सवाल उठता है कि शासन-प्रशासन को यह पता रहता है कि अप्रैल-मई में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद होनी है, फिर इसका प्रबंध पहले से क्यों नहीं कर लिया जाता?
देश में किसानों की मेहनत और जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के उपायों के चलते कृषि पैदावार लगातार बढ़ रही है। अबतक हरियाणा और पंजाब ही गेहूं उत्पादन में अग्रणी प्रदेश माने जाते थे लेकिन अब मध्य-प्रदेश, बिहार, उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में भी गेहूं की रिकार्ड पैदावार हो रही है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, दालें और मोटे अनाज व तिलहन शामिल हैं। इस पैदावार को 2020-21 तक 28 करोड़ टन तक पहुंचाने का सरकारी लक्ष्य था, जो इसबार 29.19 करोड़ टन अनाज पैदा करके पूरा कर लिया गया है। आबादी की जरूरत के हिसाब से यह 7 करोड़ टन ज्यादा है। लेकिन अब मध्य-प्रदेश के साथ साथ पूरा देश बारदाना और इसके भंडारण के संकट से जूझ रहा है। लाखों टन खुले में पड़ा गेहूं बारिश से भीगकर सड़ गया है। बारदाना उपलब्ध कराने की जवाबदारी केंद्र सरकार की है लेकिन यह कोई बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकारें चाहें तो वे भी बारदाना खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु लालफीताशाही के चलते हरेक साल इस समस्या से दो-चार होना पड़ता है। जबकि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो अचानक टूट पड़ती हो।
साठ के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के साथ ही अनाज भण्डारण की समस्या भी सुरसा मुख बनती रही है। एक स्थान पर बड़ी मात्रा में भंडारण और फिर उसका सरंक्षण अपने आप में एक चुनौती भरा और बड़ी धनराशि से हासिल होने वाला लक्ष्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनाज की पूरे देश में एकसाथ खरीद, भंडारण और फिर राज्यवार मांग के अनुसार वितरण का दायित्व भारतीय खाद्य निगम के पास है। जबकि भंडारों के निर्माण का काम केंद्रीय भण्डार निगम संभालता है। इसी तर्ज पर राज्य सरकारोंं के भी भण्डार निगम हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजादी के 72 साल बाद भी बढ़ते उत्पादन के अनुपात मे केंद्र और राज्य, दोनों ही स्तर पर अनाज भण्डार के मुकम्मल इंतजाम नहीं हुए हैं।
एफसीआई की कुल भण्डारण क्षमता बमुश्किल 738 करोड़ टन है। इसमें किराए के भण्डार गृह भी शमिल हैं। यदि सीडब्लूसी और निजी गोदामों को भी जोड़ लिया जाए तो यह क्षमता 12.5 करोड़ टन अनाज-भण्डारण की है। किसानों के वोट के लालच में राज्य सरकारें जिस हिसाब से समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद कर रही हैं, उस कारण कई करोड़ टन अतिरिक्त अनाज खरीद लिया जाता है। नतीजतन समुचित भण्डारण नमुमकिन हो जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं के साथ अन्य अनाजों की भी बंपर पैदावार हुई है। सरकार बिना बोरों के ही गेहूं खरीद रही है। नतीजतन बेमौसम हुई बारिश ने लाखों टन गेहूं खराब कर दिया। केन्द्र सरकार यदि दूरदृष्टि से काम लेती तो गोदामों में पहले से भरे अतिरिक्त अनाज को निर्यात करने की छूट दे सकती थी? इससे जहां गोदाम खाली हो जाते, वहीं व्यापारियों को दो पैसे कमाने का अवसर मिलता? यदि इसी अनाज को पंचायत स्तर पर मध्यान्ह भोजन, बीपीएल एवं एपीएल कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए स्थानीय स्तर पर ही सस्ती दरों में उपलब्ध करा दिया जाता तो भंडारण की समस्या कम हो जाती। किंतु ऐसा लगता है सड़े अनाज से शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए अनाज सड़ाने का इंतजाम नौकरशाही एक सोची-समझी मंशा से हर साल कर देती है।
भण्डारण की ठीक व्यवस्था न होने के कारण कई साल से डेढ़ से दो लाख टन अनाज खराब हो रहा है। यह एफसीआई के कुल भण्डारण का एक तिहाई हिस्सा बैठता है। इस अनाज से एक साल तक दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा सकता है। यह गोदामों की कमी की बजाय भण्डारण में बरती जाने वाली लापरवाहियों के चलते भी होता है। दरअसल कई मर्तबा एफसीआई अपने गोदाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किराए पर उठा देती है। इन कारणों से कंपनियों का माल तो सुरक्षित हो जाता है लेकिन गरीबों का भोजन सड़ने को खुले में छोड़ दिया जाता है। दरअसल कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की अनाज भण्डारण से लेकर वितरण तक की नीतियां परस्पर विरोधाभासी हैं। इनके चलते उत्पादक उपभोक्ता एवं व्यापारी तीनों लाचार हैं। जवाबदेही के लिए जिम्मेदार प्रशासक इन खामियों पर व्यवस्था की कमी जताकर पर्दा डालने का काम करते हैं। इन नीतियों को आमूलचूल बदलने की जरूरत है। यदि भारतीय खाद्य निगम विकेंद्रीकृत खाद्य नीति अपनाए तो ग्राम स्तर पर भी अनाज भण्डारण के श्रेष्ठ उपाय किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसी अनूठी भण्डारण की तकनीकें प्रचलन में हैं, जिनमें रखा अनाज बारिश, बाढ़, चूहों व कीटाणुओं से बचा रहता हैै। बिहार, असम, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश में बाढ़ से अनाज को बचाने के लिए किसान इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अनाज-भण्डारण की एक नई तकनीक भी कुछ साल पहले इजाद हुई है। इस तरकीब से वायुरहित ऐसे पीपे (सोलो बैग) तैयार किए गए हैं, जिनमें अनाज का भण्डारण करने से अनाज पानी व कीटों से शत-प्रतिशत सुरक्षित रहता है।
गांव में अनाज खरीदकर एफसीआई उसके भण्डारण की जिम्मेदारी किसानों को सौंप सकती है। किसान के पास अनाज सुरक्षित बना रहे इसके लिए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को किराया दिया जाए। यदि ऐसे उपाय अमल में लाए जाते हैं तो सरकार ढुलाई, लदाई, उतराई के खर्च से बचेगी। साथ ही अनाज के यातायात में जो छीजन होता है, वह भी नहीं होगा। इस सिलसिले में विडंबना है कि मध्य-प्रदेश में ही गेहूं भंडारण के लिए एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जा रहा है। राजगढ़ का गेहूं 250 किलोमीटर दूर होशंगाबाद में भेजा गया है। इसी तरह उज्जैन, सतना, कटनी सहित 10 ऐसे जिले हैं, जिनका गेहूं 300 किमी दूर भेजा गया है। ऐसा गोदामों में पिछले साल का अनाज भरा होने के कारण किया गया है। तय है, इस परिवहन में हजारों टन गेहूं बोरों में भराई, ट्रकों में लदाई व उतराई में नष्ट हो जाएगा।
सरकार प्रति वर्ष करीब 584 रुपए प्रति क्विंटल खाद्यान्न, फल और सब्जियों के रखरखाव पर खर्च करती है। लेकिन भण्डारण में किसान की कोई भूमिका तय नहीं है। यदि सरकार किसान के पास ही सुरक्षित रखने के लिए आर्थिक मदद करे तो इस उपाय से न केवल उचित भण्डारण होगा, बल्कि अन्नदाता किसान, फसल की सुरक्षा अपनी संतान की तरह करेगा। क्योंकि उसके द्वारा उपजाये अनाज में खून-पसीने की मेहनत लगी होती है। बहरहाल, पंचायत स्तर पर भंडारण को नीतिगत मूर्त रूप दिया जाता है तो कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी नगण्य रह जाएंगी। लेकिन हमारे देश में फिलहाल ग्रामीण, किसान और मजदूर से जुड़ा विकेंद्रीकृत नीतिगत सुधार मुश्किल है। क्योंकि नीतियों में भंडारण संबंधी सुधार किए जाते हैं तो विरोधाभास व विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी और व्यापारियों, मंडियों के कर्मचारियों व कंपनियों को लाभ पहुंचाने का गणित गड़बड़ा जाएगा? लिहाजा लालफीताशाही भंडारण संबंधी सुधारों में सबसे बड़ा रोड़ा है।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)



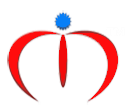 Medha Innovation & Development
Medha Innovation & Development