रामराज के आदर्श मूल्य

डॉ. विजय अग्रवालजो प्राप्ति यानी राज्याभिषेक किसी भी व्यक्ति के जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि होती है वही राम को बंधनकारी लग रही है। जंजीर, हथकड़ी, फिर चाहे वह सोने की ही क्यों न बनी हुई हो, होती तो हथकड़ी ही है। राम राजसिंहासन को इसी रूप में देख रहे थे। वे इसे इस रूप में ले रहे थे कि इसका अर्थ होगा जीवन की स्वाभाविक स्थितियों से विलग हो जाना। इसका अर्थ होगा-अपनी ही जमीन से, अपने ही लोगों से कट जाना। इसका अर्थ होगा-राजकीय विधि-विधानों से जकड़ जाना। उनकी परेशानी यह थी कि जिसकी पत्नी पृथ्वी हो उसे मर्यादा में तो रखा जा सकता है, लेकिन गुलाम बनाकर, बंधनों में जकड़कर कैसे रखा जाए। सच मानिए तो राम के इस रूप पर, इस भाव पर सहज ही विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। राम के मन की इस स्थिति में हमें व्यक्तित्व के विकास का एक अन्य सूत्र मिलता है और यह सूत्र है स्वतंत्रता का, बंधविहीनता का। लेकिन उस स्वतंत्रता या बंधनमुक्ति को सही तरीके से न समझने पर गड़बड़ी होने की पूरी-पूरी संभावना निकल आएगी। यहां राम ने जिसे बंधन माना है वह किसी अनुशासन, किसी मर्यादा या नैतिक मूल्यों का बंधन नहीं है। जो स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम कहलाए हों वे मर्यादा को बंधन भला कैसे मान सकते हैं। वे तो अपने आचरण से पुरानी मर्यादाओं को नए संदर्भो में परिभाषित कर रहे थे।उनके लिए जो सबसे बंधनकारी वस्तु थी, वह राजगद्दी थी, राजतिलक था। तभी तो उन्हें इसकी सूचना पाकर दुख हुआ था। वे यह तो मानते थे कि राजसिंहासन आवश्यक है, क्योंकि इसी से समाज की व्यवस्था बनी रहती है। किसी न किसी को तो इस पर बैठना ही होगा और अपने दायित्वों को निभाना भी होगा, क्योंकि जिसके राच्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित रूप से नर्क को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह एक चुनौती का पद है और राम को चुनौती से कोई भय भी नहीं है, लेकिन इसकी एक सीमा तो है ही। सीमा यह है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद आपके कार्यक्षेत्र की सीमा सिमटकर अपनी राजनीतिक सीमाओं तक रह जाती है। जबकि राम की इच्छा 'बड़काजू' की है। उन्हें केवल अपनी अयोध्या की प्रजा के लिए ही काम नहीं करना है, बल्कि इस धरती की प्रजा के लिए काम करना है। विश्वामित्र के साथ जाकर राम देख आए थे कि अयोध्या के बाहर के हालात क्या हैं? हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि राम ने सोचा कि यदि पृथ्वी के हित के लिए ही काम करना है तो क्यों न पहले पृथ्वी की पुत्री यानी कि सीता का वरण किया जाए। सीता यानी जनकसुता के वरण का मतलब केवल संतति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि राम ने ऐसा करके एक प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करने के दायित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था।फिर यह भी कि राम की दृष्टि में राजगद्दी कर्मक्षेत्र की अपेक्षा भोग का क्षेत्र अधिक है। वह विलासिता का हाट है, बजाय कर्म की रणभूमि के। बाद में गौतम बुद्ध ने भी अपने तरीके से इसी सिद्धांत को माना था। बुद्ध भी राजकुमार थे और अपने पिता की इकलौती संतान थे। उनके तो पिता की एक ही पत्नी थी इसलिए रामचरित मानस जैसे विवाद की वहां कोई संभावना थी ही नहीं, इसके बावजूद उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि राजगद्दी के द्वारा जनकल्याण, विश्वकल्याण को साध पाना असंभव है। हां, राजकल्याण भले ही सध जाए। अन्यथा राजा बनने के बाद अच्छे-अच्छे नियम-कानून बनाकर, अच्छी-अच्छी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करके वे कुछ कर सकते थे। और यह सच भी है कि कुछ न कुछ तो हो ही जाता। कितना? थोड़ा सा। लेकिन कब तक के लिए? कुछ समय के लिए। च्यादा नहीं हो पाता। हमेशा-हमेशा के लिए नहीं हो पाता। राम इसे हमेशा-हमेशा के लिए करना चाहते थे। गौतम बुद्ध भी यही चाहते थे।अब आप ही देख लीजिए कि राच्याभिषेक के बाद राम की कथा में बचता ही क्या है, सिवाय इसके कि रामराच्य में चारो ओर सुख और शांति छाई हुई है। इसके बाद न तो घटनाएं हैं, और न ही एक्शन। सब कुछ थम गया है। आप कल्पना करके देखें कि यदि यही स्थिति उस समय स्थापित हो गई होती, जब राम का राच्याभिषेक होना था तब क्या हुआ होता। राम दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि राजतिलक होते ही सब कुछ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए उन्हें यह घटना बेहद बंधनकारी लगने लगी और उनका मन इससे छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। और उन्हें छुटकारा पाने का मौका मिला कैकेई के दो वरदानों से। प्रकृति भी अपने आपमें विचित्र है। राम राजगद्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन राजगद्दी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। राम के पीछे-पीछे वैसे ही भागती है, जैसे कि शरीर के पीछे परछाई। राम वन को चले गए हैं। सोच रहे होंगे कि पीछा छूटा, लेकिन पीछा छूटा कहां। भरत चल दिए राजगद्दी को लेकर राम के पीछे-पीछे। भैया, लो संभालो अपना ये जंजाल। मुझसे नहीं संभलने वाला। राम ने बड़ी तसल्ली से भरत को समझाया और इस समझाने के केंद्र में रहा पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म। यहां राम पूरी तरह सही थे, सौ फीसदी खरे। इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि महाराज दशरथ ने कैकेई के प्रथम वरदान को स्वीकार करते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भरत को राजगद्दी सौंप दी थी। यहां राम ने राच्य के उत्तराधिकारी के च्येष्ठ पुत्र के सिद्धांत के स्थान पर पिता की इच्छा की सर्वोपरिता के सिद्धांत की स्थापना की। तभी तो यहां राम कह रहे हैं कि यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों की सम्मति भी यही है कि राजतिलक उसी का होता है जिसे पिता देता है।इस प्रकार हम देखते हैं कि राम ने राजगद्दी को एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार ठुकराया है। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें दो मौके ऐसे मिले जब वे अपना राजतिलक करवा सकते थे। यहां 'मौके मिले' की जगह 'प्राप्त किया' शब्द अधिक सही होगा, क्योंकि ये उन्हें किसी ने दिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने हासिल किए थे। पहला था बालि वध के बाद किष्किंधापुर का राच्य तथा दूसरा रावण-वध के बाद सोने की लंका की राजगद्दी। उन्होंने इन्हें भी ठुकराया। ये बातें उनकी दृष्टि में राच्य की निस्सारता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि केवल अपने लिए, सबके लिए नहीं। अन्यथा उन्होंने वन में आए हुए भरत से कहा ही कि मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयष, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें।[दखल][लेखक डॉ. विजय अग्रवाल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं]



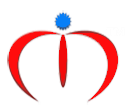 Medha Innovation & Development
Medha Innovation & Development